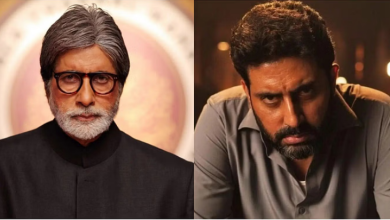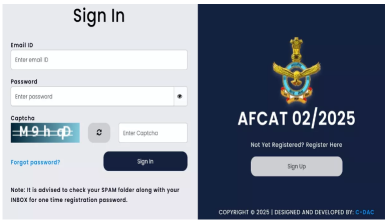कुछ तो है जिसकी परदादारी है

 सरकार ने न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता का शंख बजाया है, जो कि सराहनीय ही है। विशेष रूप से न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है और इस सवाल पर न्यायपालिका से सरकार की ठनी हुई है। संसद से पारित एक विधेयक के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका अधिक शक्तिशाली हो जाने के प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही अपने एक फैसले में रद्द कर दिया। फिर भी नियुक्तियों में पारदर्शिता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार जारी रखने की व्यवस्था कर दी है। यह एक आशाजनक पहल ही मानी जानी चाहिए।
सरकार ने न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता का शंख बजाया है, जो कि सराहनीय ही है। विशेष रूप से न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है और इस सवाल पर न्यायपालिका से सरकार की ठनी हुई है। संसद से पारित एक विधेयक के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका अधिक शक्तिशाली हो जाने के प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही अपने एक फैसले में रद्द कर दिया। फिर भी नियुक्तियों में पारदर्शिता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार जारी रखने की व्यवस्था कर दी है। यह एक आशाजनक पहल ही मानी जानी चाहिए।
हाल ही में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून बने दस साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर हमें पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्यों में निहित अंतर्विरोधों को आंख से ओझल नहीं होने देना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक तरफ तो सरकार के प्रभावशाली नेता-मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी सत्ता के गलियारों में पारदर्शिता बढ़ने के बजाय घटने की स्थिति पर ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं। दु:खद स्थिति तो यह है कि केंद्र और कुछ प्रदेशों की सरकारों ने सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर ही जंजीरें डाल दी हैं। पारदर्शिता की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर ही पहरे लगाए जा रहे हैं। सबसे मजेदार स्थिति तो राजस्थान की है।
सनद रहे कि सूचना के अधिकार के आंदोलन में राजस्थान अग्रणी रहा है। यही नहीं, वर्ष 1977-78 में भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्वकाल में ही यहां सूचना के अधिकार की पहल हो गई थी। बाद में ईमानदार और सुशिक्षित समाजसेवी अरुणा राय के नेतृत्व में हजारों शिक्षित-अशिक्षित लोगों ने सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार का कानून बना।
लेकिन उसी राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सत्ता में आने के बाद पिछले डेढ़ बरस में सूचना अधिकार आयुक्तों का दफ्तर ही सूना हो गया है और सूचना मांगने के सैकड़ों आवेदन फाइलों में पड़े धूल खा रहे हैं। वजह यह है कि राज्य सूचना आयोग के लिए 10 आयुक्तों में से नौ स्थान कई महीनों से खाली पड़े हैं। सरकार की मंशा लगती है कि ‘न रहेगा सुनने वाला आयुक्त और न ही होगी सुनवाई।”
हाल ही में सूचना का अधिकार कानून की दसवीं सालगिरह पर आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा – ”सरकार से सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र में आस्था पैदा करता है।”” लेकिन उनकी सरकार आने के बाद केंद्र में भी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति महीनों तक लटकी रही। यही नहीं, सूचना मांगने के आवेदनों की हजारों फाइलों पर तो अभी तक विचार ही नहीं किया जा सका है। सरकार द्वारा जारी अधिकृत आंकड़ों के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत आए करीब नौ लाख 62 हजार आवेदन फिलहाल विचाराधीन हैं। कहा जा सकता है कि इस संख्या में निरंतर इजाफा होने वाला है।
यों देश में इस अधिकार के प्रति लगातार बढ़ रही जागरुकता का ही यह परिणाम है कि इन दस वर्षों में सूचना के अधिकार का उपयोग करने वाले नागरिकों की संख्या 80 लाख तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ सरकारी नेताओं और अफसरों का कष्ट बढ़ता जा रहा है। वे सूचना को छिपाने, दबाने, आवेदन को विभिन्न् विभागों में घुमाने के हथकंडे अपनाने लगे हैं। इसका सबसे कारगर जवाबी फॉर्मूला यह है कि ”फिलहाल यह जानकारी शीर्ष स्तर पर पहुंची फाइलों में है। उपलब्ध होने पर सूचित किया जाएगा।”” आलम यह है कि संबंधित मंत्रालयों के मंत्री या भाजपा के सांसदों को ही कई जानकारियां नहीं मिल पातीं।
सूचना-प्रसारण और वित्त मंत्री अरुण जेटली न्यायपालिका में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में उनके अपने मंत्री साथियों को मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची के प्रस्तावों का विस्तृत विवरण पहले नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है कि सरकार को अपनों से ही ‘लीक” होने का खतरा लगता है। इसलिए बैठक में पहुंचने पर ही कई मंत्रियों को प्रस्तावों की पूरी जानकारी मिल पाती है। इसका नफा-नुकसान यह होता है कि बैठक में प्रधानमंत्री या उनके द्वारा अनुमति प्राप्त वरिष्ठ मंत्री ही विचाराधीन विषयों पर अपनी बात रख पाते हैं। मंत्रियों को केवल उनकी बातें सुनने की सुविधा है। कार्यसूची के प्रस्तावों का विवरण पहले मिलने पर ही तो मंत्रिगण पहले से ही सोच-समझकर कुछ राय दे सकते हैं अथवा सवाल कर सकते हैं। अन्यथा कुछ मिनटों की बैठक में नए मुद्दों पर फटाफट अपनी राय कोई मंत्री कैसे दे सकता है। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और पं. जवाहरलाल नेहरू तक के प्रधानमंत्रित्वकाल में मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कार्यसूची के प्रस्तावों के विवरण भेजे जाते रहे हैं, ताकि मंत्रिगण बैठक में खुलकर अपनी राय व्यक्त कर सकें। लेकिन जब मंत्रियों को ही कोई निर्णय ले लिए जाने के बाद सूचना पाने का अधिकार होगा तो अनुमान लगाया जा सकता है कि आमजन के लिए कितनी पारदर्शिता होगी?
लोकतांत्रिक प्रावधान यह है कि संसद या विधानसभाओं में विचार के लिए आने वाले महत्वपूर्ण प्रस्तावित विधेयकों-कानूनों का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए, ताकि कोई भी सामान्य नागरिक उन पर अपनी राय प्रस्तुत कर सके। भाजपा सरकार आने के बाद आया घरेलू हिंसा रोकथाम विधेयक सीधे संसद में पेश हुआ था। जबकि करोड़ों लोगों के सामान्य जीवन को कानूनी परिधि में लाने वाली व्यवस्था पर पहले सार्वजनिक बहस एवं राय की गुंजाइश होती है।
यह तर्क भी दिया जा रहा है कि अब देश में ‘डिजिटल क्रांति” हो गई है। इसलिए विभिन्न् मंत्रालयों की सूचनाएं निविदाएं प्राप्ति से स्वीकृति तक की जानकारी नेट पर उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन असलियत यह है कि सरकारी मंत्रालयों के नेट सर्वर पर बोझ होने से दो-दो दिन तक संबंधित विभागों की सूचनाएं खुल ही नहीं पातीं। यही नहीं कुछ मंत्रालयों के अधिकारी बड़ी चतुराई से अंतिम समय में सूचनाएं वेबसाइट पर डालते हैं, ताकि कम लोगों तक ही जानकारी पहुंचे। इससे भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की गुंजाइश बन जाती है। फिर विभिन्न् क्षेत्रों में सक्रिय लोग क्या प्रतिदिन सभी मंत्रालयों-विभागों की वेबसाइट की सार्वजनिक सूचनाएं देख सकते हैं? महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहले की तरह कम खर्च पर अखबारों में भी देने से क्या पारदर्शिता का अधिक लाभ नहीं मिल सकेगा? बहरहाल, लोकतंत्र में सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं होने की अपेक्षा निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए।