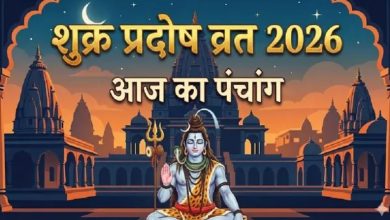ईश्वर भक्ति से खुलता है मुक्ति का द्वार, इन बातों को जरूर करें आत्मसात

कर्म और वासनाओं का जटिल जाल जीव को संसार में बांधता है लेकिन जब हम अपनी ऊति को मोह-वासनाओं और अहंकार से हटाकर ईश्वर की ओर लगाते हैं तो यह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। अत मनुष्य को अपनी ऊति को मोह वासनाओं और अहंकार से हटाकर ईश्वर की ओर लगाना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है और मुक्ति का मार्ग है।
सत्व, रज और तम के अतिरेक से जब यह चराचर सृष्टि प्रकट हुई, तब विराट पुरुष ने इसके 10 मुख्य आधार स्थापित किए, जो स्वयं जीवन-दर्शन व प्रबंधन के सूत्र बन गए। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के दशम अध्याय में शुकदेवजी कहते हैं :
“अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमीतयः।
मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः।।”
सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशनुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये केवल विषय नहीं, अपितु मानव जीवन को परमात्मा की ओर उन्मुख करने वाले सोपान हैं। इनमें से प्रथम पांच पर भाव-विचार प्रस्तुत है :
सर्ग : सर्ग का तात्पर्य है भगवत-प्रेरणा से पंचभूतों, तन्मात्राओं, दस इंद्रियों, अहंकार और महत्तत्व की उत्पत्ति। यह वह आदिम रचना है, जहां से सब कुछ प्रकट हुआ।
दार्शनिक सार : हम स्वयं को परम सत्ता की अद्भुत सृष्टि का एक अभिन्न अंग मानें। हमारा अस्तित्व एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित है। हमारा आचार, विचार और व्यवहार लोकोपकारी और निष्काम हो, जिससे हम इस विराट सृष्टि के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा सकें। जैसे एक नन्हा बीज भी विशाल वृक्ष का आधार बन सकता है, वैसे ही हमारा एक नेक कर्म भी पूरे समाज को पोषित कर सकता है।
विसर्ग: विसर्ग ब्रह्माजी द्वारा रचित वह सृष्टि है, जो विभिन्न रूपों में दृश्यमान और गतिशील है। कोई बड़ा है, कोई छोटा; कोई धनी है, कोई निर्धन।
दार्शनिक सार : जीवन की विविधता हमें सिखाती है कि विषमता में भी समता और कटुता में भी मधुरता का अनुभव किया जा सकता है। यह सृष्टि अपनी विविधता से परिपूर्ण है, फिर भी एक ही सूत्र में बंधी है। हमें भी जीवन में भिन्नता को स्वीकार कर, उसमें अभिन्नता और प्रेम खोजना चाहिए।
स्थान: स्थान का अर्थ है प्रतिपल लय हो रही सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखना। यह मर्यादा धर्म और न्याय की सुप्रतिष्ठा से ही संभव है। भगवत्कृपा ही इस संतुलन को बनाए रखती है।
दार्शनिक सार: जब स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत होकर हम अन्याय-अनीति करते हैं, तो यह संपूर्ण व्यवस्था डगमगा जाती है। जीवन में संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना अनिवार्य है। यह तथ्य सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो समाज हम देते हैं, वही हमें वापस मिलता है। हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार, एक प्रतिध्वनि है, जो हमारे पास लौटकर आती है।
पोषण: पोषण का अभिप्राय है भगवान का अपने भक्तों का प्रतिपालन और संकटों से उनकी रक्षा करना। यह भगवान की करुणा का साक्षात रूप है।
दार्शनिक सार : सहानुभूति और करुणा मानव मूल्यों के मूल हैं। हमें भी दूसरों का सहारा बनना चाहिए। जिस प्रकार एक नदी अपनी धारा से जीवन देती है, उसी प्रकार हमें अपनी करुणा से दूसरों के जीवन को गति और मति देनी चाहिए। संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करना, उसके जीवन को पोषण देना, यही सच्चा मानवीय धर्म है।
ऊति : ऊति का शाब्दिक अर्थ है संकल्प, प्रेरणा या बुना हुआ ताना-बाना। दार्शनिक दृष्टि से यह कर्म और वासनाओं का जटिल जाल है, जो जीव को संसार में बांधता भी है और मुक्त भी करता है।
दार्शनिक सार : वासनाएं पिछले जन्मों से अर्जित प्रवृत्तियां हैं, जो वर्तमान जीवन में व्यवहार को प्रभावित करती हैं। कर्म वे कार्य हैं जो प्राणी अपनी वासनाओं के अनुसार करते हैं। ये कर्म अच्छे या खराब हो सकते हैं और उनके परिणाम भी उसी के अनुसार होते हैं।
कर्म के परिणामस्वरूप, प्राणी को सुख-दुख का अनुभव होता है। वासनाओं के कारण वे जन्म-मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, लेकिन जब यह संकल्प (ऊति) धर्म और भक्ति की ओर मुड़ता है, तो मुक्ति का द्वार खोलता है।
कर्म और वासनाओं का जटिल जाल जीव को संसार में बांधता है, लेकिन जब हम अपनी ऊति को मोह-वासनाओं और अहंकार से हटाकर ईश्वर की ओर लगाते हैं, तो यह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। अत: मनुष्य को अपनी ऊति को मोह, वासनाओं और अहंकार से हटाकर ईश्वर की ओर लगाना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है और मुक्ति का मार्ग है।