इंदिरा गांधी के इस फैसले से बदल गई थी देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था
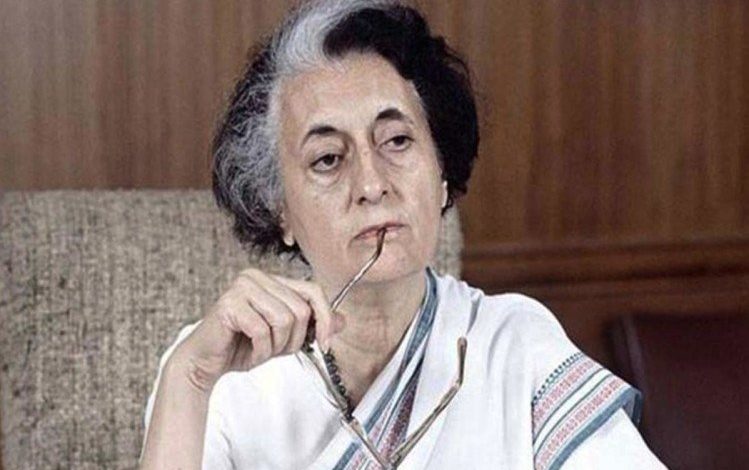
आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। आज से 103 साल पहले 19 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंदिरा का जन्म हुआ था। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। जनवरी 1966 से लेकर मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से लेकर अक्तूबर 1984 (जब इंदिरा की हत्या हुई) तक देश की प्रधानमंत्री रहीं।
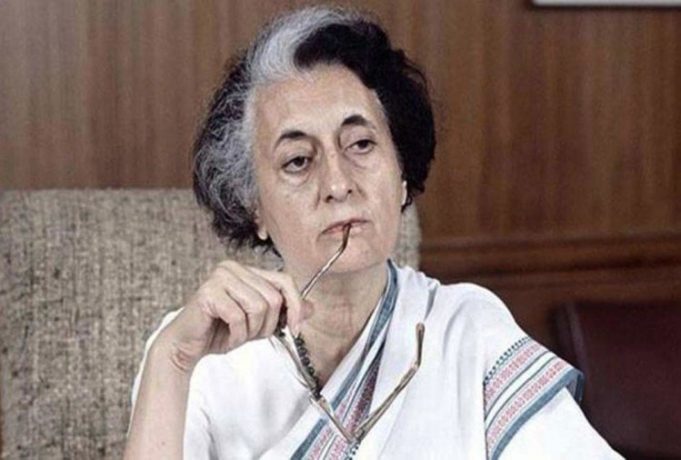
इंदिरा और आपातकाल के बारे में तो पूरा देश जानता है। आज उनके जन्मदिवस के मौके पर हम आपको इंदिरा के उस एक फैसले के बारे में बता रहे हैं, जिसने पूरे भारत की बैंकिंग व्यवस्था ही बदल दी। आगे की स्लाइड्स में पढ़ें।
आज से करीब 51 साल पहले.. 19 जुलाई 1969 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले ने देश की पूरी बैंकिंग प्रणाली बदल दी थी। जब इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आज भी वह फैसला बैंकों को प्रभावित कर रहा है।
क्या होता है राष्ट्रीयकरण? इंदिरा ने क्यों लिया था ये फैसला? बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश पर क्या हुआ असर? इन सवालों के जवाब आगे की स्लाइड्स में पढ़ें।
राष्ट्रीयकरण को सरल भाषा में सरकारीकरण भी कह सकते हैं। जब किसी संस्था या व्यापारिक इकाई का स्वामित्व सरकार के अधीन होता है, तो उसे राष्ट्रीयकृत संस्था या इकाई कहा जाता है। ऐसी संस्थाओं पर सरकार का स्वामित्व तब ही माना जाता है जब उसकी पूंजी का न्यूनतम 51 फीसदी हिस्सा सरकार के पास हो।
भारत में सबसे पहला राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) था। इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में ही कर दिया गया था।
फिर 1958 में एसबीआई के सहयोगी बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया।
सबसे बड़े पैमाने पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी ने किया। 14 बड़े बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ।
इसके बाद 1980 में राष्ट्रीयकरण का दौर चला। जब सात बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया।
बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
देना बैंक
यूको बैंक
सिंडिकेट बैंक
केनरा बैंक
इलाहाबाद बैंक
यूनाइटेड बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रीयकरण की मुख्य वजह बड़े व्यवसायिक बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली ‘क्लास बैंकिंग’ नीति थी। बैंक केवल धनपतियों को ही ऋण व अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाते थे।
इन बैंकों पर ज्यादातर बड़े औद्योगिक घरानों का आधिपत्य था।
कृषि, लघु व मध्यम उद्योगों, छोटे व्यापारियों को सरल शर्तों पर वित्तीय सुविधा देने, आम लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण किया गया।
आर्थिक तौर पर सरकार को लग रहा था कि कॉमर्शियल बैंक सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में सहायक नहीं हो रहे थे।
विशेषज्ञों के अनुसार, उस समय देश के 14 बड़े बैंकों के पास देश की करीब 70 फीसदी पूंजी थी। लेकिन इनमें जमा पैसा सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा था, जहां लाभ के अवसर ज्यादा थे।
हालांकि कुछ जानकार इंदिरा के इस फैसले को राजनैतिक अवसरवादिता भी मानते हैं। उनके अनुसार, 1967 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं, तो पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत नहीं थी।
कहा जाता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखने से लोगों में संदेश गया कि इंदिरा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाली प्रधानमंत्री हैं।
जिस अध्यादेश के जरिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव लाया गया, उसका नाम था ‘बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस’। बाद में इसी नाम से विधेयक पारित हुआ और कानून बना।
विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
‘क्लास बैंकिंग’ की नीति ‘मास बैंकिंग’ मे बदल गई। यानी आम लोगों को भी ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाएं मिलने में आसानी हुई।
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का बड़े पैमाने पर और तेजी से विस्तार हुआ।
आंकड़ों पर गौर करें, तो जुलाई 1969 में देश में बैंकों की कुल 8322 शाखाएं थीं। 1994 तक ये आंकड़ा 60 हजार से ज्यादा पहुंच गया।
बैंकों के पास काफी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ। जिसे कर्ज के रूप में दिया गया।
छोटे उद्योग, कृषि और छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जैसे क्षेत्रों को फायदा हुआ।
सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को लोन पोर्टफोलियो में 40 फीसदी कृषि लोन की हिस्सेदारी का निर्देश दिया।
बैंकों की शाखाएं बढ़ने से देश में इस क्षेत्र में रोजगार के मौके भी बढ़े।







