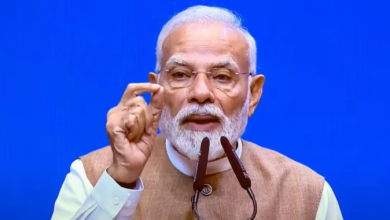विशेष आलेख: 90 साल में भी युवा संघ

न ब्बे वर्ष की आयु में स्वाभाविक वृद्धावस्था होती है। लेकिन यदि अपवाद स्वरूप इस आयु में स्वस्थ, चंचल, बलशाली, युवा हो तो विरोधाभास लगता है। संस्थाएं बनती हैं और बुढ़ी होकर इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। इसके अनगिनत उदाहरण हैं। इनमें पूर्व सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर भारत का साम्यवादी और समाजवादी आंदोलन शामिल है। स्वयं कांग्रेस पार्टी 100 वर्ष पूरा करते-करते पतझड़ का सामना करने लगी थी। इन साक्ष्यों के बीच एक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने अपना चरित्र बदल लिया। मूल पिंड को छोड़कर वह परकाया में प्रवेश कर जीवित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। नब्बे साल में इसकी ऊर्जा और इसके सामने चुनौतियां दोनों ही इसकी युवावस्था को प्रतिबिम्बित करती हैं। इसकी भूमिका इतिहास बनती रही है परन्तु यह स्वयं वर्तमान का हिस्सा बना रहता है। आखिर ऐसी कौन सी संजीवनी है जो इसे ऊर्जावान और प्रगतिमान बनाए रखती है? इस प्रश्न का उत्तर न तो जटिल है न ही कठिन। यह भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद को परिभाषित और परिष्कृत करना ही इसका बुनियादी सिद्धांत है।
ब्बे वर्ष की आयु में स्वाभाविक वृद्धावस्था होती है। लेकिन यदि अपवाद स्वरूप इस आयु में स्वस्थ, चंचल, बलशाली, युवा हो तो विरोधाभास लगता है। संस्थाएं बनती हैं और बुढ़ी होकर इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। इसके अनगिनत उदाहरण हैं। इनमें पूर्व सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर भारत का साम्यवादी और समाजवादी आंदोलन शामिल है। स्वयं कांग्रेस पार्टी 100 वर्ष पूरा करते-करते पतझड़ का सामना करने लगी थी। इन साक्ष्यों के बीच एक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने अपना चरित्र बदल लिया। मूल पिंड को छोड़कर वह परकाया में प्रवेश कर जीवित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। नब्बे साल में इसकी ऊर्जा और इसके सामने चुनौतियां दोनों ही इसकी युवावस्था को प्रतिबिम्बित करती हैं। इसकी भूमिका इतिहास बनती रही है परन्तु यह स्वयं वर्तमान का हिस्सा बना रहता है। आखिर ऐसी कौन सी संजीवनी है जो इसे ऊर्जावान और प्रगतिमान बनाए रखती है? इस प्रश्न का उत्तर न तो जटिल है न ही कठिन। यह भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद को परिभाषित और परिष्कृत करना ही इसका बुनियादी सिद्धांत है।
यूरोप की थोपी गई परिभाषा भारतीय राष्ट्रवाद को शक्तिहीन और अस्मिताविहीन बनाता है। संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने इस सत्य को सिद्धांत बना दिया कि भारत एक सभ्यता का वाहक है। कल तक सभ्यता राष्ट्र की पालना थी आज राष्ट्र सभ्यता को अपने गर्भ में नवजात शिशु की तरह पोषित कर रही है। इसी सभ्यताई राष्ट्र को डॉ. हेडगेवार ने हिन्दू राष्ट्र कहा। जिनका विखंडित भारत और अहिन्दूकरण ही लक्ष्य है वे संघ और इसके सिद्धांत के सभ्यताई मिशन को साम्प्रदायिक करार देते रहे हैं। यह नई बात नहीं है। स्थापना के मात्र पांच वर्षों के बाद 1930 में साम्राज्यवादी सरकार ने इसमें ‘आतंकी खतरे’ का बीज देखना शुरू किया था और 1932-33 में इसे ‘साम्प्रदायिक’ व ‘फासीवादी’ कहकर इस पर प्रतिबंध लगाने का जोखिम उठाया था। कारण था संघ का महत्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी। ब्रिटिश खुफिया दस्तावेज के अनुसार इस भागीदारी ने विदर्भ में मृत आंदोलन में जान फूंकने का काम किया था। लेकिन साम्राज्यवादी सरकार को तब मुंह की खानी पड़ी जब 1934 में मध्य प्रांत (तब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का संयुक्त नाम था) विधान परिषद में गैर सरकारी पक्ष के जिन 14 सदस्यों ने सरकार के इस कदम पर बहस में हिस्सा लिया सबने इसका विरोध किया। संघ का प्रतिनिधि विधान परिषद में नहीं था परन्तु संघ के राष्ट्रवाद की छाया वहां थी। अंततः सरकार को अपने कदम खींचने पड़े।
1942 के आंदोलन के दौरान स्वयंसेवकों का दमन इस हद तक बढ़ गया कि उनके पत्रों को भी जब्त किया जाने लगा और उनके कारण उनके परिवार को प्रताडि़त किया जाने लगा। ऐसा सैंकड़ो उदाहरण हैं। मद्रास में रेलवे क्लर्क और संघ के मुख्य शिक्षक लक्ष्मीनारायण मूर्ति का पत्र जब्त किया गया और उनके परिवार पर कहर ढाया गया।
संघ की बढ़ती शक्ति के साथ ही इसके सामने राजनीतिक चुनौतियां भी आई। आजादी से पूर्व हिन्दू महासभा संघ शक्ति का उपयोग अपने राजनीतिक मिशन के लिए करना चाहती थी। परन्तु उसे निराशा हाथ लगी। इसका राष्ट्रवाद व्यक्ति से समूह तक की परिकल्पना है। अर्थात् नीचे से ऊपर की ओर न कि ऊपर से नीचे की ओर। अतः व्यक्ति अहम हो जाता है। व्यक्ति के चिंतन, सोच-समझ और दायरे में परिवर्तन का अभियान किसी एक पीढ़ी से शुरू होकर दूसरी पीढ़ी तक समाप्त नहीं होता है। भविष्य जिसका लक्ष्य हो पीढि़यों के साथ संवाद जिसकी उत्कंठा हो वह दीर्घायु तो होगा परन्तु वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को डॉ. हेडगेवार ने ‘संगठन के लिए संगठन’ कहा।
स्वतंत्रता के पश्चात् विमर्श की प्रकृति में एक नया आयाम आया। यद्यपि संघ अपेक्षाकृत छोटा संगठन था परन्तु इसका वैचारिक प्रभाव इसकी तुलना में कई गुणा अधिक था। समय और संदर्भ के अनुसार इसकी भूमिका बदलती है परन्तु हिन्दू राष्ट्र का वैचारिक अधिष्ठान सरसंघचालक मोहन भागवत के अनुसार अपरिवर्तनीय बना रहता है। नये विमर्श ने संघ-विरोधवाद को जन्म दिया। संघ से मतान्तर रखने वाले राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकतें तीनों हैं जो इसे अपने प्रतिकूल पाती है। इन ताकतों ने धारणा की राजनीति शुरू की। इसका पहला कदम था संघ के साथ संवाद समाप्त करना। इसे वैचारिक अछूत बनाकर रखना। लेकिन संघ इससे विचलित नहीं हुआ। इसके तर्क की ताकत इसे प्रभावी बनाती गयी। सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यों से उपजी ऊर्जा का प्रभाव भारत के राजनीतिक और वैचारिक जीवन दोनों में हुआ। संघ की प्रेरणा से राजनीतिक हस्तक्षेप 1950 से शुरू हुआ। देश का राजनीतिक व्याकरण सहज रूप में रहा है। साथ ही धर्मनिरपेक्षता पुनर्परिभाषित हो रही है। कल्पना कीजिए अगर संघ की स्थापना नहीं हुई होती तो समकालीन भारत का स्वरूप क्या होता? विमर्श कैसा होता? भारत की संस्कृति, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को किस रूप में देखा जाता? हीन भावना ग्रंथी को मिटाकर ‘मैं कौन हूं’ को स्पष्टता से परिभाषित करने का काम संघ करता है।
सभ्यता के दौर में परिष्कार का कार्य कभी विराम नहीं लेता है न ही प्रदूषण का खतरा कभी कम होता है। समाज, संस्कृति और राजनीति तीनों को नए-नए प्रदूषण के कारकों एवं ताकतों से सामना करना पड़ता है। यह व्यक्तिवाद से लेकर अराजकतावाद, हिंसा से लेकर संस्कृति क्षरण, आर्थिक-सामाजिक असमानता से लेकर बाजारवाद के खतरे हैं। जो संस्था राष्ट्र से साक्षात्कार करती है वह प्रतिदिन नयेपन के साथ चीजों को देखती है और चुनौतियों से जुझती है। संघ का कार्य परिष्कार करना है जो कभी नहीं समाप्त होने वाला कार्य है। निराशावाद से यह कभी ग्रस्त नहीं हुआ। अबतक संघ सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नों से रूबरू होता रहा। अब इसके सामने वे आर्थिक व राजनीतिक प्रश्न हैं जिससे देश की दीर्घकालिक चरित्र प्रभावित होता है। इसे दलित विमर्श से लेकर नवउदारवाद के प्रश्नों को समाधानात्मक रूप से देखना है। संवाद और संघर्ष इसका माध्यम है। इस नये संदर्भ में संघ का नया रूप आता है। इसलिए यह सतत् अजीवन बना रहता है। जब इसके संस्थापक डॉ. हेडगेवार की मृत्यु हुई तब यह भय उत्पन्न हुआ कि संघ बिखर जाएगा, इसकी गति धीमी हो जाएगी। परन्तु ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगी। समाचारपत्र ‘मराठा’ ने 23 अगस्त जुलाई, 1940 को मुख्य पृष्ठ पर शीर्षक दिया “हेडगेवार का संघ अब भी मजबूत होता जा रहा है।” 2015 में हम यह कह सकते हैं कि डॉ. मोहन भागवत का संघ प्रबल होता जा रहा है।