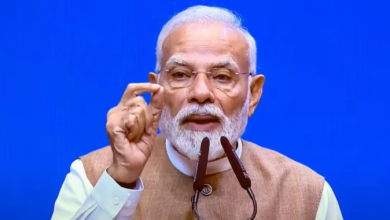विकास की नीतियां बदलने का वक्त – यशवंत सिन्हा

भा रत में घोषित आर्थिक सुधारों का इतिहास 24 साल पुराना है, लेकिन इन 24 वर्षों में भी सुधारों को लेकर जो विवाद हैं, वे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स (जैसे गार अथवा पिछली तिथि से लागू होने वाले कर) विदेशी पूंजी निवेश इत्यादि अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आज भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। जब डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार कहा था कि आर्थिक सुधारों पर भी उसी प्रकार की राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए जिस प्रकार की सहमति राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में विद्यमान है। लेकिन खेद है कि ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। सबसे अधिक कष्ट तो हमें तब होता है जब हमारे राजनीतिक दल सत्ता में रहते हुए एक प्रकार की सोच रखते हैं और विपक्ष में बिलकुल दूसरे प्रकार की।
रत में घोषित आर्थिक सुधारों का इतिहास 24 साल पुराना है, लेकिन इन 24 वर्षों में भी सुधारों को लेकर जो विवाद हैं, वे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स (जैसे गार अथवा पिछली तिथि से लागू होने वाले कर) विदेशी पूंजी निवेश इत्यादि अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आज भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। जब डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार कहा था कि आर्थिक सुधारों पर भी उसी प्रकार की राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए जिस प्रकार की सहमति राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में विद्यमान है। लेकिन खेद है कि ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। सबसे अधिक कष्ट तो हमें तब होता है जब हमारे राजनीतिक दल सत्ता में रहते हुए एक प्रकार की सोच रखते हैं और विपक्ष में बिलकुल दूसरे प्रकार की।
यही कारण है कि वर्ष 1991 के बाद जितनी सरकारें केंद्र में रही हैं, उन्होंने मजबूती के साथ आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया है और विपक्ष में रहते हुए उसका उतना ही पुरजोर विरोध भी किया है। बहुत गंभीरता से इस विषय पर सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आर्थिक सुधारों का विरोध करना आसान इसलिए हो जाता है कि इन सुधारों के चलते गरीबों के जीवन में तत्काल कोई विशेष अंतर नहीं आता है और इसलिए देश के गरीबों को उकसाना बहुत आसान हो जाता है। यह सही भी है कि आर्थिक सुधारों का लाभ गरीबों तक तत्काल नहीं पहुंचता है। सुधारों की दिशा मुख्य रूप से और आवश्यक रूप से आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के बारे में होती है। विकास दर बढ़ने से देश को बहुत सारे लाभ होते हैं। गरीबों को भी नियोजन प्राप्त होता है लेकिन तत्काल नहीं। दूसरी ओर गरीब रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, नियोजन जैसे मुद्दों से जूझता रहता है। वह इन समस्याओं का तत्काल समाधान चाहता है।
विकास के ये दो पहलू यानी कि आर्थिक विकास दर में वृद्धि तथा आम लोगों की जीवनशैली में सुधार को एक साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश इस दिशा में हमारे देश में नारे तो बहुत बने, लेकिन धरातल पर उसके अनुरूप सोच मजबूती से नहीं उतर पाई। ताजा नारा है इनक्लूसिव ग्र्रोथ यानी समावेशी विकास का इसी बीच हमारे देश में अमीरों-गरीबों के बीच की खाई बढ़ती चली गई।
टीवी के माध्यम से गरीबों को भी अमीरों की सर्वसुखसंपन्न् जीवनशैली का नित्य प्रतिदिन दर्शन होने लगा। उनके अंदर भी अपनी जीवनशैली में सुधार लाने की उत्कट अभिलाषा पैदा हुई। कुछ लोग शहर की ओर भागे। जो गांव ही में छूट गए उसमें से कई लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया और समाज में चारों तरफ एक कोलाहल का वातावरण पैदा हो गया। हम सब लोग, जो कभी न कभी शासन में रहे हैं, उन्होंने देश की अधिकांश जनता के साथ न्याय नहीं किया है।
स्पष्ट है कि देश में जिस प्रकार की नीतियां केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा पिछले सात दशकों में चलाई गईं, वे नाकाम हो चुकी हैं। अगर हम आगे भी उसी ढर्रे पर चलते रहे तो आगे भी हमें असफलता ही हासिल होगी इसलिए सोच को बदलना आवश्यक है। अत: लाख टके का सवा यह है कि सरकारों को अब क्या करना चाहिए?
2 मई, 2015 को मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा था जिसमें मैंने सुझाव दिया था कि भारत सरकार को दो योजनाएं शुरू करनी चाहिए। एक, प्रधानमंत्री ग्राम पुनर्निर्माण योजना और दूसरी, प्रधानमंत्री श्रम सुधार योजना। मैंने पत्र में यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए उस योजना पर कम से कम 50 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करना चाहिए। इसकी व्यवस्था हम आसानी से मनरेगा तथा नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमपेंट फंड से कर सकते हैं। सिंचाई की उपलब्धता से हमारे देश के किसानों के जीवन में जो फर्क देखने को मिलेगा उसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे भरपूर सहायता मिलेगी।
ग्रामीण जनता की जीवनशैली में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि देश के हर गांव को जोड़ने के लिए एक पक्की सड़क हो, खेतों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, सबके पास घर हो, बिजली हो, साफ पीने का पानी हो, शौचालय और स्वच्छता हो, हरेक गांव में कम से कम एक प्राइमरी स्कूल हो तथा हर दो किलोमीटर के भीतर एक स्वास्थ्य केंद्र हो।
इन्हीं सब सुविधाओं को शहरों की झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी उपलब्ध करवाया जाए। हमें यह सब करने का एक नया तरीका खोजना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि हमें इन योजनाओं के लिए भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों या सीधे पंचायतों को 100 प्रतिशत राशि उपलब्ध करानी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर यह योजना भी गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूले पर आधारित नहीं होकर हर राज्य की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। आवश्यकता का आकलन करने के लिए देश के 6 लाख गांवों में सरकार के तीन प्रतिनिधियों की एक टोली जानी चाहिए। हर टोली के पास एक प्रपत्र होना चाहिए, जिसमें बिजली, पानी इत्यादि सुविधाओं का जिक्र होना चाहिए। टोली का काम केवल टिक करना होगा। गांव में यदि सड़क है तो टोली हां को टिक करेगी, नहीं है तो टोली नहीं को टिक करेगी। इस प्रकार हर गांव का एक सर्वे हो जाएगा और सबसे पिछड़े गांवों तथा क्षेत्रों की जानकारी भी। ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में सरकारी सेवक काम करते हैं। यदि सावधानी से इन टोलियों का निर्माण किया जाए तो अधिक से अधिक एक महीने के भीतर हमें हर गांव के बारे में सारी आवश्यक सूचना मिल जाएगी और उसके बाद योजना को क्रियान्वित करने में विलंब नहीं होगा।
इस प्रकार की प्रणाली शहरी झुग्गी-झोपडिय़ों में भी अपनाई जानी चाहिए। जीवनशैली में सुधार लाने के साथ ही साथ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इन योजनाओं के चलते प्रचुर मात्रा में नियोजन के अवसर भी पैदा होंगे। गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो पाएगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक विकास दर में वृद्धि के माध्यम से ही देश आगे बढ़ेगा, पर देश की जनता तब आगे बढ़ेगी, संतुष्ट होगी और आर्थिक सुधारों का स्वागत करेगी, जब हम शीघ्र से शीघ्र उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें और उनके बच्चों के लिए रोजगार के अवसर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराएं।
– See more at: http://naidunia.jagran.com/editorial/sampadikya-now-its-time-to-change-development-policy-486537#sthash.J34mT74m.dpuf