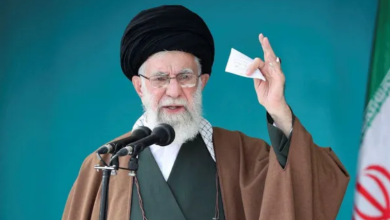आज भी 30 देशों की महिलाएं ‘खतना’ सहने को मजबूर

शाजिया याद करती हैं कि जब वह 7 साल की थीं तो उनकी मां उन्हें चॉकलेट दिलाने के बहाने एक घर के पिछवाड़े में एक अंधेरे से कमरे में ले गई थीं। उसे कसकर पकड़ लिया गया। फिर उसके बाद उसे बस असहनीय दर्द ही याद है। वह घर आते हुए पूरा रास्ता रोती रही थी। उन्हें अगले 20-25 साल तक समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या था। फिर उसे महिला खतना के बारे में पता चला। यह किसी एक महिला की आपबीती नहीं है। दुनिया भर के 30 देशों में हर साल करीब 20 करोड़ बच्चियों या लड़कियों को खतना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

इनमें से आधी से ज्यादा सिर्फ तीन देशों – मिस्र, ईथियोपिया और इंडोनेशिया में हैं। पत्रकार आरेफा जोहरी उन लड़कियों में से हैं, जिन्हें सात साल की उम्र में खतना की पीड़ादायक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा था। भारत में शिया मुस्लिम के बेहद संपन्न और शिक्षित समुदाय दाउदी बोहरा में इस प्रथा का रिवाज है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सह संस्थापक जाकिया सोमान का इस बारे में कहना है, ‘खतना जैसी प्रथाएं अमानवीय और गैर इस्लामी हैं। ये महिलाओं पर होने वाली हिंसा को बढ़ावा देती हैं, इन्हें तत्काल बंद किया जाना चाहिए।’
आमतौर पर छह सात साल की उम्र में और बेहोशी की दवा दिए बिना ही लड़कियों का खतना किया जाता है। पिछड़े इलाकों में खतने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लेड या छुरी से उनके स्वास्थ्य को अक्सर गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। साफ औजारों का इस्तेमाल ना होने के कारण इन लड़कियों को जीवन भर कई तरह के संक्रमण झेलने पड़ सकते हैं। आज इस प्रथा के खिलाफ कई स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। बोहरा समुदाय की इस लड़ाई में कई गैर बोहरा भी पूरा साथ दे रहे हैं। दिल्ली की स्वतंत्र फिल्कार प्रिया गोस्वामी भी उनमें से एक हैं। प्रिया को 2013 में महिला खतना की प्रथा पर बारीकी से रोशनी डालती अपनी फिल्म ‘अ पिंच ऑफ स्किन’ के लिए प्रतिष्ठित वृत्तचित्र फिल्म निर्माण का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।

प्रिया ने एक पत्रिका में लड़कियों के खतने के बारे में पढ़ने के बाद इस विषय पर फिल्म बनाने का फैसला किया। प्रिया कहती हैं, ‘इस समुदाय से ना होने के कारण इसकी तह तक पहुंचना कठिन था, लेकिन मैंने हर हाल में इस विषय को सामने लाने का फैसला किया। इस पर फिल्म बनाने का फैसला कॉलेज में मेरे द्वारा लिखित एक नाटक चक्रव्यूह का ही विस्तार था, जिसमें कई धर्मों की पितृसत्तात्मक परंपराओं को उठाया गया था। खतना भी ऐसी ही परंपराओं में से एक है।’
सात साल की उम्र में इस प्रक्रिया से गुजर चुकीं पत्रकार और खतना प्रथा के खिलाफ काम कर रहीं कार्यकर्ता आरेफा के नजरिए से इस प्रथा के विषय को उठाने के लिए 2014 में प्रिया को ‘आईएडब्ल्यूआरटी लॉन्ग डॉक्युमेंट्री ग्रांट 2015’ दिया गया। प्रिया कहती हैं, ‘बोहरा समुदाय की आरेफा के लिए अपनी पहचान को सामने लाकर अपने समाज की इस प्रथा के खिलाफ खड़े होना एक बड़ा कदम था।’
प्रिया और आरेफा समेत मुंबई, बोस्टन और हॉन्गकॉन्ग की पांच महिलाओं ने इस प्रथा के खिलाफ अभियान को दिशा देने के मकसद से संगठन साहियो शुरू किया। प्रिया बताती हैं, ‘इस प्रथा को निभाने के पीछे आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि इससे महिलाओं में अत्यधिक यौनेच्छा नियंत्रित रहती है, जिसके कारण शादी से पूर्व उनकी पवित्रता बनी रहती है और शादी के उपरांत वे अवैध विवाहेतर संबंधों से दूर रहती हैं और अपने पति के प्रति उनकी वफादारी कायम रहती है। यही कारण देकर लड़कियों के मां-बाप को यह भरोसा दिलाया जाता है कि इस प्रथा को निभाना उनकी बेटियों के हित में है। यहूदियों, इसाइयों, मुसलमानों और कई अन्य धर्मों में इसे एक धार्मिक आवश्यकता माना जाता है।’
आरेफा कहती हैं, ‘यौनेच्छा नियंत्रित करने के तर्क से विपरीत कुछ समुदाय यह दावा भी करते हैं कि इससे महिलाओं की प्रजजन क्षमता और कामेच्छा में इजाफा होता है और साथ ही वे इसे शरीर के इन अंगों की साफ सफाई के लिए भी जरूरी मानते हैं।’ साहियो ने दाउदी बोहरा समुदाय में खतना को लेकर एक ऑनलाइन सर्वे किया, जिसमें दुनियाभर से बोहरा समुदाय के 385 लोगों ने हिस्सा लिया और उनमें से 81 प्रतिशत लोगों ने इस प्रथा के खत्म होने की इच्छा जताई। बोहरा समुदाय की कुछ महिलाओं ने इसी कड़ी के तहत पिछले साल इस प्रथा के खिलाफ चेंज डॉट ओआरजी पर एक याचिका दायर की, जिसे भरपूर समर्थन मिल रहा है।

अब तक इस पर 82,685 हस्ताक्षर आ चुके हैं। फिल्मकार और बाल अधिकार कार्यकर्ता इंसिया दरिवाला भी इन महिलाओं में शामिल हैं। इंसिया खुशकिस्मत रहीं कि अपनी मां के प्रयास से वह इस प्रथा से बच गईं, लेकिन उनकी बहन समेत उनके परिवार की अन्य सभी लड़कियों को इससे गुजरना पड़ा। इंसिया कहती हैं, ‘खतना के खिलाफ आवाज उठाकर और यह बताकर ही इसे रोका जा सकता है कि यह धार्मिक परंपरा नहीं है। यह लड़कियों के हित में नहीं है और अपने शरीर पर लड़कियों के अधिकार का उल्लंघन है।’ इंसिया कहती हैं इस प्रथा के खिलाफ अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और अब बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देशों में खतना के खिलाफ कानून हैं। कई अफ्रीकी देश भी इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। हाल ही में नाइजीरिया और गाम्बिया में इस प्रथा के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया गया। केन्या में 2011 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत में इसे लेकर कोई कानून नहीं है। संयुक्त राष्ट्र खतने की प्रथा को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानता है।
क्या है खतना ??
फीमेल जेनिटल कटिंग या फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी खतना में महिलाओं के बाह्य जननांग के कुछ हिस्से को काट दिया जाता है। इसके तहत क्लिटोरिस के ऊपरी हिस्से को हटाने से लेकर बाहरी और भीतरी लाबिया को हटाना और कई समुदायों में लेबिया को सिलने की प्रथा तक शामिल है। एक सामाजिक रीति के रूप में इस प्रथा की जड़ें काफी गहरी हैं और इसे बेहद आवश्यक माना जाता है। यूनिसेफ के आंकड़े कहते हैं कि जिन 20 करोड़ लड़कियों का खतना होता है, उनमें से करीब साढ़े चार करोड़ बच्चियां 14 साल से कम उम्र की होती हैं और इनमें से सबसे अधिक तीन देशों – गांबिया, मॉरितानिया और इंडोनेशिया की होती हैं।
किताब ‘द हिडन फेस ऑफ ईव’ में लेखिका नवल अल सादावी कहती हैं, ‘खतना के पीछे धारणा यह है कि लड़की के यौनांगों के बाहरी हिस्से के भाग को हटा देने से उसकी यौनेच्छा नियंत्रित हो जाती है, जिससे यौवनावस्था में पहुंचने पर उसके लिए अपने कौमार्य को सुरक्षित रखना आसान हो जाता है।’ सादावी को खतना की सबसे दुष्कर विधि ‘इनफिबुलेशन’ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था जिसमें वजाइना के बाह्य हिस्से को काट दिया जाता है और मासिक धर्म और अन्य शारीरिक स्रावों के लिए थोड़े से हिस्से को छोड़ कर शेष भाग को सिल दिया जाता है।