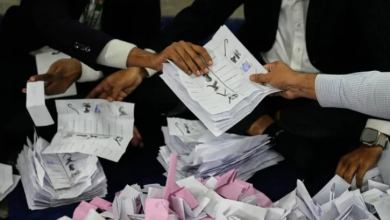ईरान ने 21 जून की सुबह अमेरिका के शक्तिशाली जासूसी ड्रोन ट्राइटन को मार गिराया और कहा कि वह ईरानी क्षेत्र में था। इसकी कीमत 1260 करोड़ रुपये बताई जा रही है और अमेरिका इसे मार गिराने को उकसावे का कदम मान रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह दूसरी घटना है जब अमेरिकी ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है।

अमेरिका की दलील है कि ड्रोन ईरान के क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान की बहुत बड़ी गलती कहा है और पता चला है कि ईरान की कार्रवाई को लेकर अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर सलाह ले रहा है।
वहीं ईरानी सेना के कमांडर हुसैन सलामी ने दावा किया कि अमेरिकी ड्रोन ईरान की हवाई सीमा में था। इसलिए, उसे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिरा दिया गया। उन्हेंने कहा कि ईरान किसी पर भी हमला नहीं करेगा। लेकिन, जो उसकी सीमा में घुसेगा, उसे तबाह कर दिया जाएगा।
ड्रोन गिराने की घटना ऐसे समय में हुई है, जब मीडिया रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। इसे देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेताया है कि हमला करने की गलती न करें। उधर, सऊदी अरब ने ईरान से कहा कि जब आप शिपिंग में दखल देंगे तो ऊर्जा की आपूर्ति प्रभावित होगी। ऐसे में तेल की ऊंची कीमतों का असर विश्व के हर व्यक्ति पर पड़ेगा।
क्या आप जानते हैं कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी की वजह क्या है और इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई थी।
1970 में शुरू हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी

यह तनातनी लगभग चार दशक पहले शुरू हुई थी, जब 1971 में यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टीटो, मोनाको के प्रिंस रेनीअर और राजकुमारी ग्रेस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति सिप्रो अग्नेयू और सोवियत संघ के स्टेट्समैन निकोलई पोगर्नी ईरानी शहर पर्सेपोलिस में जुटे थे। इस पार्टी का आयोजन ईरानी शाह रजा पहलवी ने किया था। पार्टी के आठ साल बाद ईरान में नए नेता अयतोल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी का आगमन हुआ और उन्होंने इसे शैतानों का जश्न कहा था।
1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले खुमैनी तुर्की, इराक और पेरिस में निर्वासित जीवन जी रहे थे। खुमैनी, शाह पहलवी के नेतृत्व में ईरान के पश्चिमीकरण और अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता के लिए उन्हें निशाने पर लेते थे। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग को अपदस्थ कर पहलवी को सत्ता सौंप दी थी। मोहम्मद मोसादेग ने ही ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था और वो चाहते थे कि शाह की शक्ति कम हो।
किसी विदेशी नेता को शांतिपूर्ण वक्त में अपदस्थ करने का काम अमेरिका ने पहली बार ईरान में किया था। लेकिन यह आखिरी नहीं था। इसके बाद अमेरिका की विदेश नीति का यह एक तरह से हिस्सा बन गया। 1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्तापलट किया उसी का नतीजा 1979 की ईरानी क्रांति थी। इन 40 सालों में ईरान और पश्चिम के बीच कड़वाहट खत्म नहीं हुई।
इस्लामिक रिपब्लिक ईरान से चार दशकों की असहमति का नतीजा यह मिला कि न तो ईरान ने घुटने टेके और न इलाके में शांति स्थापित हुई। यहां तक कि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद से दुश्मनी और बढ़ गई है।
सत्ता पाते ही खुमैनी की उदारता में आया परिवर्तन

सत्ता में आने के बाद उग्र क्रांतिकारी खुमैनी की उदारता में अचानक से परिवर्तन आया। उन्होंने खुद को वामपंथी आंदोलनों से अलग कर लिया और विरोधी आवाजों को दबाना तथा कुचलना शुरू कर दिया। क्रांति के परिणामों के तत्काल बाद ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो गए। तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में लेकर 52 अमेरिकी नागरिकों को एक साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा था। कहा तो यह भी जाता है कि इस घटना को खुमैनी का मौन समर्थन प्राप्त था।
इन सबके बीच सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान और इराक के बीच आठ सालों तक युद्ध चला। इसमें लगभग पांच लाख ईरानी और इराकी सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था। यहां तक कि सोवियत यूनियन ने भी सद्दाम हुसैन की मदद की थी।
माना जाता है कि इराक ने इस युद्ध के दौरान ईरान पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। यही वह समय था जब ईरान ने परमाणु बम की संभावनाओं की तलाश शुरू की थी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2002 तक गुपचुप तरीके से चल रहा था।
अगले कुछ वर्षों में अमेरिका और ईरान के संबंधों में कड़वाहट कुछ कम होती दिखी। बराक ओबामा ने इसके लिए 2015 में ज्वॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया था। लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही एकतरफा फैसला लेते हुए इस समझौते को रद्द कर दिया। साथ ही ईरान पर कई नए प्रतिबंध भी लगा दिए गए।
ट्रंप ने न केवल ईरान पर प्रतिबंध लगाए बल्कि दुनिया के देशों को धमकी देते हुए कहा कि जो भी इस देश के साथ व्यापार जो करेगा वो अमेरिका से कारोबारी संबंध नहीं रख पाएगा। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच भी मतभेद सामने आ गए।
ईरान पर लगे प्रतिबंध और इसके मायने
अमेरिका ने ईरान पर वो सभी प्रतिबंध दोबारा लगा दिए हैं जिन्हें साल 2015 में हटा लिया गया था। उल्लेखनीय है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ था जिसके तहत ईरान से ये प्रतिबंध हटा लिये गए थे। अमेरिका का मानना था कि आर्थिक दबाव के कारण ईरान नए समझौते के लिये तैयार हो जाएगा और अपनी हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगा देगा।
क्या हैं प्रतिबंध?
- ईरान सरकार द्वारा अमेरिकी डॉलर को खरीदने या रखने पर रोक।
- सोने या अन्य कीमती धातुओं में व्यापार पर रोक।
- ग्रेफाइट, एल्युमीनियम, स्टील, कोयला और औद्योगिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर पर रोक।
- ईरान की मुद्रा रियाल से जुड़े लेन-देन पर रोक
- ईरान सरकार को ऋण देने से संबंधित गतिविधियों पर रोक।
- ईरान के ऑटोमोटिव सेक्टर पर प्रतिबंध।
- इन सबके अलावा ईरानी कालीन तथा खाद्य पदार्थों का आयात भी बंद कर दिया जाएगा।
- अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई भी कंपनी या देश इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो उन्हें इसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
5 नवंबर 2018 से लगाए गए प्रतिबंध

I
- ईरान के बंदरगाहों का संचालन करने वालों पर प्रतिबंध।
- ऊर्जा, शिपिंग और जहाज़ निर्माण सेक्टर पर प्रतिबंध।
- ईरान के पेट्रोलियम संबंधित लेन-देन पर प्रतिबंध।
- सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के साथ विदेशी वित्त संस्थानों के लेन-देन पर प्रतिबंध।
- प्रतिबंधों का प्रभाव
दोबारा लगाए गए प्रतिबंध न केवल अमेरिकी नागरिकों और व्यवसायों पर लागू होते हैं, बल्कि गैर-अमेरिकी व्यवसायों या व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य द्वारा ईरान से संबंधित व्यापार और निवेश गतिविधि में शामिल उन सभी लोगों को दंडित करना है जिन्हें इन प्रतिबंधों के तहत कोई विशेष छूट प्राप्त नहीं है। कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले से ही अपने ईरानी व्यवसाय बंद कर दिये हैं या ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं।
ईरान पर लगे प्रतिबंधों का भारत पर असर

चीन के बाद भारत ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। वहीं, ईरान भी अपने दस प्रतिशत तेल का निर्यात केवल भारत को ही करता है। भारत के लिये यह एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ जहाँ ईरान के साथ उसके गहरे संबंध हैं वहीँ दूसरी ओर, वह ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने के फ़ैसले से भी सहमत नहीं है। भारत पर इस समय अमेरिकी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिये भी निवेश किया है जो भारत-अफगानिस्तान के बीच एक महत्त्वपूर्ण लिंक है। अमेरिकी प्रतिबंध इस परियोजना के विकास में बाधा डाल सकते हैं।
जापान और दक्षिण कोरिया ने ईरान से तेल आयात को या तो रोक दिया है, या बिल्कुल कम कर दिया है। ईरान में उत्पादित कुल कच्चे तेल का दस फीसदी भारत आयात करता है। ईरान से तेल खरीदने में भारत को फायदा भी है, क्योंकि उसे भुगतान के लिए मनचाहा वक्त मिल जाता है।
ईरान परमाणु समझौता क्या था?
ईरान परमाणु समझौता इस दशक की वह महत्वपूर्ण घटना है जिससे दुनिया के तमाम देशों की विदेश नीति बड़े पैमाने पर प्रभावित होती रही है। जब इस समझौते को राष्ट्रपति ट्रंप ने खारिज किया था तो कहा था, ‘मेरे लिए यह स्पष्ट है कि हम इस समझौते के साथ रहकर ईरान के परमाणु बम को नहीं रोक सकते। ईरान समझौता मूलरूप से दोषपूर्ण है, इसलिए मैं आज ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने की घोषणा कर रहा हूं।’
समझौते की नींव
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का मानना था कि ईरान एक गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम चला रहा है। जिसका लक्ष्य मिसाइलों के लिए परमाणु हथियार बनाकर उनका परीक्षण करना है। इसके बाद अमेरिका की अगुवाई में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद ईरान की कमर टूट गई। इसके बाद पी5+1 कही जाने वाली छह शक्तियों (अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और चीन) के साथ उसकी बातचीत का लंबा दौर शुरू हुआ जिसके बाद जुलाई 2015 में वियना समझौते (ईरान परमाणु समझौते) के तहत एक संधि या समझौता हुआ था।
ईरान परमाणु समझौते की प्रमुख शर्तें

समझौते के तहत ईरान ने अपने करीब नौ टन अल्प संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करके 300 किलोग्राम तक करने की शर्त स्वीकार की थी। यह भी तय हुआ था कि ईरान अपना अल्प संवर्धित यूरेनियम रूस को देगा और सेंट्रीफ्यूजों की संख्या घटाएगा। इसके बदले में रूस ईरान को करीब 140 टन प्राकृतिक यूरेनियम येलो-केक के रूप में देगा।
यूरेनियम के इस कंपाउंड का इस्तेमाल बिजलीघरों के लिए परमाणु छड़ बनाने के लिए होता है। संधि की शर्त यह भी थी कि आईएईए को अगले 10 से 25 साल तक इस बात की जांच करने की स्वतंत्रता होगी कि ईरान संधि के प्रावधानों का पालन कर रहा है या नहीं। इन सारी शर्तों के बदले में पश्चिमी देश ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने पर सहमत हुए थे।
किसकी मजबूरी था यह समझौता
अमेरिका सहित दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए भी यह समझौता करना उतना ही जरूरी हो गया था जितना कि ईरान के लिए। मध्य-पूर्व के बदलते समीकरणों ने अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ा दी थी। अमेरिका के दुलारे सऊदी अरब ने इस्लाम की जिस वहाबी विचारधारा को पाला-पोसा था, उससे इस्लामिक स्टेट (आईएस) का जन्म हुआ और आईएस कितना बड़ा संगठन था यह पेरिस से लेकर अमेरिका तक हुए आतंकी हमलों से साफ हो चुका था।
उस समय आईएस से निपटने की कोशिश में अमेरिका इस्लाम के उस शिया मत के हाथ मजबूत करना चाहता था जो न सिर्फ अपेक्षाकृत लचीला माना जाता है बल्कि आईएस के निशाने पर भी था। ईरान शिया जगत का नेतृत्व करता है। अमेरिका को उम्मीद थी कि इससे आईएस को हराना आसान हो जाएगा।
क्या आसान होगा अमेरिका-ईरान युद्ध
अमेरिका ने मध्य-पूर्व में अपनी सेना और साजो-सामान की तैनाती की है। इसके साथ ही इराक में मौजूद अपने गैर-महत्वपूर्ण राजनयिक कर्मचारियों की संख्या भी घटा दी है। इराक के साथ युद्ध के बाद ईरान ने अपनी सैन्य शक्तियों में काफी इजाफा किया है। उसने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया। अगर डोनल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान पर युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है तो अमेरिका को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा सकता है।